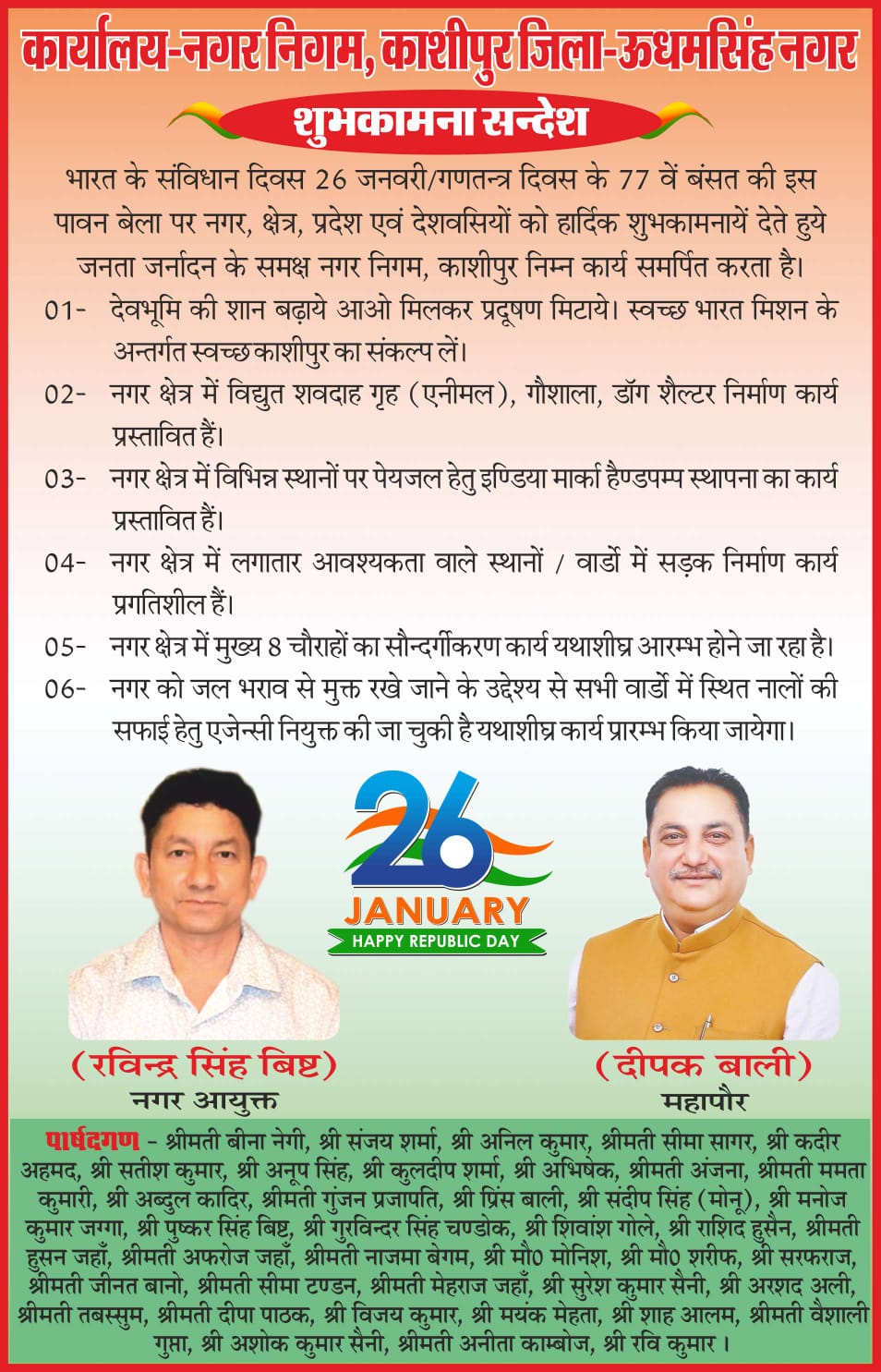भारत(सुनील कोठारी)। संविधान सभा ने जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी थी, वह व्यवस्था आने वाले समय में किस तरह के मोड़ लेगी, इसका अनुमान शायद उसके किसी भी सदस्य ने नहीं लगाया होगा। 2026 की संसद जिस स्वरूप में खड़ी दिखाई देती है, वह उस ऐतिहासिक कल्पना से टकराती हुई नजर आती है, जिसमें संसद को विचारों के टकराव, मतभेदों की अभिव्यक्ति और सत्ता को जवाबदेह बनाने का सबसे बड़ा मंच माना गया था। आज स्थिति यह है कि उसी संसद के भीतर महात्मा गांधी की छवि को बार-बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनके विचारों को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है और उनके नाम को राजनीतिक तंज का माध्यम बनाया जा रहा है। यह वही संसद है जिसने कभी गांधी के सत्य और अहिंसा को अपनी आत्मा माना था। अब उसी सदन में इतिहास को खंडित करने की होड़ दिखाई देती है, जहां अतीत को नकारना वर्तमान राजनीति की सबसे प्रभावी रणनीति बन चुका है।
आज़ादी के बाद देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्रियों को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग संसद के भीतर हो रहा है, वह भारतीय संसदीय परंपरा में एक असहज मोड़ की ओर इशारा करता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को केवल उनकी नीतियों या फैसलों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों का विषय बनाया जा रहा है। इसी क्रम में इंदिरा गांधी को भी उसी कथित ‘बदचलन’ की कड़ी में जोड़ दिया जाता है, मानो इतिहास का मूल्यांकन अब विचारों से नहीं, चरित्र हनन से किया जाएगा। यह रवैया न केवल उन नेताओं की विरासत को चुनौती देता है, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़ा करता है, जिसने संसद को गरिमापूर्ण संवाद का स्थान माना था। यहां तक कह दिया गया कि पहले के किसी भी प्रधानमंत्री के पास देश को गढ़ने की कोई दृष्टि नहीं थी, जैसे भारत का निर्माण किसी सामूहिक प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक अकेले दौर की देन हो।
इसी राजनीतिक माहौल में जब संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती है, तो विपक्ष की भूमिका लगातार सिमटती हुई दिखाई देती है। मौजूदा समय में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के भीतर बोलने की अनुमति न मिलना केवल एक प्रक्रियात्मक विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़ा सवाल बन जाता है। संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों को बिना रोक-टोक बोलते देखा जाता है, तीखे आरोप लगाए जाते हैं, अतीत के नेताओं पर टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जब विपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता है, तो उसे मौन रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। यह स्थिति यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या संसद अब केवल बहुमत का मंच बन चुकी है, जहां असहमति को जगह देना जरूरी नहीं समझा जाता। जब नेता प्रतिपक्ष तक को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता, तो फिर आम सांसदों की आवाज़ का क्या महत्व रह जाता है।
लोकतंत्र की आत्मा सवाल पूछने और जवाब मांगने में निहित होती है, लेकिन मौजूदा हालात में यह आत्मा लगातार दबाव में दिखाई देती है। संसद वह स्थान होती है जहां जनता की समस्याएं, उसकी चिंताएं और उसकी अपेक्षाएं आवाज़ पाती हैं। जब यह आवाज़ ही नियंत्रित कर दी जाए, तो लोकतांत्रिक ढांचा खोखला होने लगता है। देश के लाखों लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में अपनी जान दी थी, ताकि भविष्य में भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन अब यह भावना कमजोर पड़ती नजर आती है। 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, पर उस सपने के साथ यह संकेत भी जुड़ा है कि विकास की इस यात्रा में सवाल पूछने वालों के लिए जगह सीमित होती जा रही है। यह विकास किस कीमत पर होगा, इस पर चर्चा करने की गुंजाइश लगातार घट रही है।
इन परिस्थितियों के बीच लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की भूमिका भी लगातार बहस के केंद्र में आ गई है। स्पीकर को संसद का निष्पक्ष संरक्षक माना जाता है, जो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए समान रूप से नियम लागू करता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा स्पीकर की कार्यशैली में यह संतुलन दिखाई नहीं देता। इससे पहले राज्यसभा में सभापति के रूप में धनकड़ के कार्यकाल के दौरान भी ऐसे ही सवाल उठे थे, जब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि ऊपरी सदन में बोलने की स्वतंत्रता लगातार सीमित की जा रही है। उस समय भी महाभियोग की बात सामने आई थी, ताकि एक प्रतीकात्मक संदेश दिया जा सके कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। अब वही बहस लोकसभा में दोहराई जा रही है, जहां स्पीकर की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी भारत की स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। जब वैश्विक शक्तियां खुले तौर पर यह संकेत देती हैं कि भारत को किस देश से व्यापार करना चाहिए और किससे नहीं, और देश के भीतर मंत्री एक-दूसरे की ओर जिम्मेदारी डालते नजर आते हैं, तो यह छवि बनती है कि निर्णय प्रक्रिया कितनी केंद्रीकृत हो चुकी है। जब वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं और विदेश मंत्री यह कहते हैं कि वे उस सौदे का हिस्सा नहीं हैं, तो यह भ्रम केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी जाता है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि सत्ता का वास्तविक केंद्र बहुत सीमित हो गया है, और बाकी संस्थाएं केवल औपचारिक भूमिका निभा रही हैं।
इसी पृष्ठभूमि में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या किसी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करना तब आसान हो जाता है, जब विदेशी ताकतों को केवल एक व्यक्ति से संवाद करना होता है। जब वही व्यक्ति 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, तो सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा कमजोर पड़ती है। शायद यही कारण है कि संसद के भीतर स्पीकर की भूमिका को लेकर महाभियोग की चर्चा फिर से तेज हो गई है। विपक्ष का मानना है कि स्पीकर का रुख पूरी तरह सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका हुआ है और उनके फैसले उसी दिशा में जाते हैं, जिससे सत्ता को कोई असुविधा न हो। यह धारणा संसद की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
इसी क्रम में महिला सांसदों द्वारा लोकसभा के स्पीकर को लिखा गया पत्र भी राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा बन गया। उस पत्र में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को महिला सांसदों से जोड़कर उनकी जान को खतरा बताया गया, जो न केवल अपमानजनक था बल्कि तथ्यहीन भी। सांसदों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री का सदन में न आना किसी संभावित खतरे का परिणाम नहीं, बल्कि उनका स्वयं का निर्णय था। पत्र में यह भी लिखा गया कि स्पीकर पर सत्तारूढ़ दल का दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उनसे अपेक्षा की गई कि वे लोकसभा के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करें। यह पत्र अपने आप में इस बात का संकेत है कि संसद के भीतर असंतोष कितनी गहराई तक पहुंच चुका है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसद के भीतर हुई वह बहस भी अहम हो जाती है, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी खड़े होकर यह कहते हैं कि उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने स्वयं आश्वासन दिया था कि बजट चर्चा से पहले उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी का यह कहना कि स्पीकर ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अनुमति देने की बात कही थी, और उसके तुरंत बाद संसदीय मंत्री का खड़े होकर यह कहना कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया, संसद की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह केवल शब्दों का विवाद नहीं रह जाता, बल्कि यह भरोसे और संस्थागत विश्वसनीयता का संकट बन जाता है। जब सदन के भीतर सार्वजनिक रूप से यह कहा जाए कि स्पीकर अपने ही शब्दों से पीछे हट रहे हैं, तो यह स्थिति संसद की गरिमा को और कमजोर करती है। विपक्ष का कहना है कि संसद का रुख वही होगा जो मौजूदा सत्ता चाहती है, और कौन बोलेगा तथा क्या बोलेगा, यह भी सत्ता ही तय करेगी। ऐसी परिस्थिति में संसद बहस का मंच कम और नियंत्रित मंच अधिक प्रतीत होने लगती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषण ने भी इस माहौल को और अधिक तीखा बना दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए गए उनके वक्तव्य में गांधी परिवार को ‘पुश्तैनी चोर’ कहा जाना और यह आरोप लगाना कि उन्होंने महात्मा गांधी का उपनाम तक चुरा लिया, भारतीय संसदीय इतिहास में असाधारण माना जा रहा है। यह टिप्पणी केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और विरासत को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। विपक्ष का आरोप है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर संसद के भीतर मर्यादा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। यह भी सवाल उठता है कि क्या संसद में अब किसी भी स्तर की भाषा स्वीकार्य हो गई है, बशर्ते वह सत्ता के हित में हो। इस तरह की टिप्पणियां न केवल विपक्ष को निशाने पर लेती हैं, बल्कि देश के राजनीतिक संवाद के स्तर को भी प्रभावित करती हैं।
इतिहास पर हमला यहीं नहीं रुकता। संसद के भीतर जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत संबंधों पर टिप्पणी, एनी बेसेंट और मीराबेन के संदर्भों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और इंदिरा गांधी के चरित्र को लेकर बयानबाजी करना, यह सब मिलकर एक ऐसे माहौल का निर्माण करते हैं जहां अतीत को बदनाम करना वर्तमान सत्ता की रणनीति का हिस्सा बन जाता है। विपक्ष का कहना है कि यह केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश है। जब पहले के सभी प्रधानमंत्रियों को यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि उनके पास कोई दृष्टि नहीं थी, तो यह संदेश दिया जाता है कि देश का निर्माण केवल मौजूदा सत्ता के दौर में ही संभव हुआ है। यह सोच न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अन्याय है, बल्कि लोकतांत्रिक निरंतरता की अवधारणा को भी कमजोर करती है।
महाभियोग की चर्चा इसी पृष्ठभूमि में एक प्रतीकात्मक हथियार के रूप में सामने आती है। विपक्ष जानता है कि बहुमत के कारण यह प्रस्ताव सफल नहीं होगा, लेकिन इसका उद्देश्य केवल परिणाम हासिल करना नहीं है। इसका मकसद दुनिया के सामने यह संदेश रखना है कि भारत की संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं किस स्थिति में हैं। इतिहास में 1954, 1966 और 1985 में स्पीकर के खिलाफ महाभियोग की कोशिशें की गई थीं, और भले ही वे असफल रहीं हों, लेकिन वे संसदीय इतिहास में दर्ज हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह चौथा प्रयास भी केवल एक तारीख बनकर रह जाएगा, या फिर यह लोकतंत्र की स्थिति पर एक गहरी बहस को जन्म देगा। विपक्ष के सामने यह दुविधा है कि संसद के भीतर रहकर संघर्ष किया जाए या फिर बाहर निकलकर जनता के बीच अपनी आवाज़ को और तेज किया जाए।
इस बहस के केंद्र में जनता की भूमिका भी आती है। जब संसद के भीतर चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज़ दबाई जाती है, तो यह सवाल उठता है कि जनता की समस्याएं कहां रखी जाएंगी। बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक तनाव, धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते टकरावकृये सभी मुद्दे संसद में चर्चा के योग्य हैं, लेकिन जब बहस का मंच ही सीमित हो जाए, तो ये सवाल हाशिए पर चले जाते हैं। सत्ता का ध्यान इस बात पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है कि नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाए, न कि इस पर कि असहमति को कैसे समायोजित किया जाए। यह स्थिति लोकतंत्र को एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है, जहां चुनावी बहुमत ही सब कुछ तय करने लगता है और नैतिक जवाबदेही पीछे छूट जाती है।
मीडिया की भूमिका पर भी इस पूरे घटनाक्रम में सवाल उठ रहे हैं। जिसे कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था, वही मीडिया अब कई मामलों में सत्ता से सवाल पूछने से कतराता नजर आता है। प्रधानमंत्री द्वारा खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना, चुनिंदा मंचों पर ही संवाद करना और कठिन सवालों से बचना, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां सत्ता और मीडिया के बीच की दूरी कम होती दिखाई देती है। विपक्ष का आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के औजार के रूप में किया जा रहा है, ताकि असहमति की आवाज़ को कमजोर किया जा सके। इस माहौल में संसद भी उसी दबाव का हिस्सा बनती प्रतीत होती है।
अंततः सवाल यह नहीं रह जाता कि स्पीकर के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि लोकतंत्र के पास अब कौन से प्रभावी हथियार बचे हैं। जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती दिखाई दें, जब संसद में बोलने की स्वतंत्रता सीमित हो जाए और जब इतिहास को बदनाम करने की राजनीति हावी हो जाए, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। विपक्ष के सामने नैतिक चुनौती यह है कि वह जनता को कैसे भरोसा दिलाए कि लोकतांत्रिक संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं सत्ता के लिए यह परीक्षा है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल संवाद को कुचलने के लिए करेगी या उसे मजबूत करने के लिए।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इस देश में अब भी कोई ऐसा नैतिक साहस बचा है, जो कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा हो सके। क्या संसद फिर से उस स्थान में बदल सकेगी, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों बिना डर के अपनी बात रख सकें। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत की यात्रा बहस, असहमति और संवाद के जरिए आगे बढ़ी है। यदि संसद ही निष्प्रभावी हो जाती है, तो फिर लोकतंत्र का आधार क्या बचेगा। यह अंधेरा कितना गहरा है और क्या कहीं रोशनी की किरण बाकी है, यही सवाल आज भारत की राजनीति के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है।