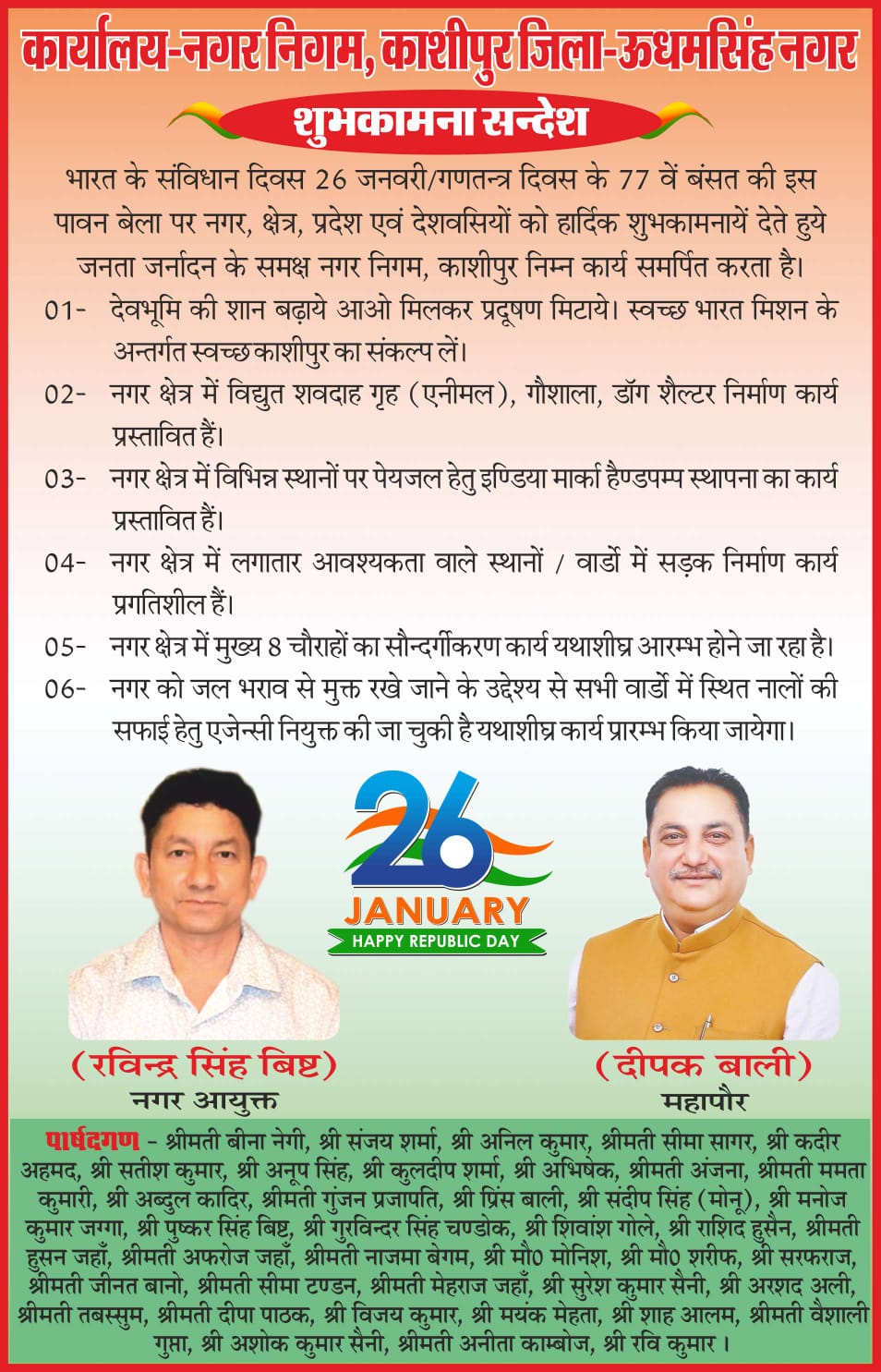नई दिल्ली(सुनील कोठारी)।नीति, कूटनीति और बाज़ार की जटिलताओं के बीच भारत और अमेरिका के बीच उभरती व्यापारिक समझ की चर्चा ने देश के भीतर एक गहरे और संवेदनशील प्रश्न को जन्म दे दिया है, जो केवल आंकड़ों, आयात–निर्यात या टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़ा है जिस पर भारत की आत्मा टिकी मानी जाती है। खेती और डेयरी को लेकर जिस “शून्य सहनशीलता” की नीति को भारत अब तक अपनी हर अंतरराष्ट्रीय डील की अडिग लक्ष्मण रेखा बताता रहा है, उसी को लेकर अब संदेह, आशंका और राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है। सरकार के उच्च स्तर से पहले ही यह दोहराया जा चुका था कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह महज़ व्यापार का विषय नहीं बल्कि करोड़ों किसानों की रोज़ी-रोटी, गांवों की सामाजिक संरचना और देश की खाद्य संप्रभुता का सवाल है। इसके बावजूद जब अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व और कृषि प्रशासन से जुड़े बयानों में भारत को एक विशाल कृषि बाज़ार के रूप में रेखांकित किया गया, तो यह चिंता स्वाभाविक रूप से गहराने लगी कि कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक लाभ की गणनाओं के बीच वही रेखा धुंधली तो नहीं की जा रही, जिसे अब तक अटल माना जाता रहा है।
भारत की कृषि व्यवस्था को समझे बिना इस बहस की गहराई को पकड़ना संभव नहीं है, क्योंकि यहां खेती केवल उत्पादन या व्यापार का क्षेत्र नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक परंपरा और ग्रामीण जीवन की आधारशिला है। देश की लगभग पचास प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है और यह निर्भरता केवल रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि भोजन, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था के पूरे चक्र को संचालित करती है। औसतन एक से दो एकड़ भूमि पर खेती करने वाला भारतीय किसान वैश्विक बाज़ार की असमान प्रतिस्पर्धा के सामने पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके विपरीत अमेरिका में कॉर्पोरेट फार्मिंग का वर्चस्व है, जहां बड़े-बड़े कृषि समूहों को सरकारी संरक्षण और अरबों डॉलर की सब्सिडी मिलती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। यदि ऐसे सब्सिडी-समर्थित कृषि उत्पाद कम या शून्य आयात शुल्क के साथ भारतीय बाज़ार में प्रवेश करते हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा समान नहीं रह जाती, बल्कि सीधे-सीधे घरेलू किसान के लिए अस्तित्व का संकट बन जाती है।
अमेरिका से संभावित सस्ते कृषि आयात को लेकर सबसे बड़ा डर “डंपिंग” का है, जहां अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों के बाज़ारों में बेहद कम कीमत पर उतार दिया जाता है। यदि गेहूं, मकई, सोयाबीन या अन्य कृषि उत्पाद भारतीय मंडियों में सस्ते दामों पर उपलब्ध होने लगते हैं, तो घरेलू फसलों की कीमतों पर तत्काल दबाव बनेगा। इसका सीधा असर किसान की आय पर पड़ेगा, जो पहले ही लागत, मौसम और बाज़ार की अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मूल्य अस्थिरता केवल एक मौसम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह किसान को कर्ज़ के चक्र में धकेल देती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती जाती है। यही कारण है कि भारत ने अब तक हर व्यापार समझौते में खेती को एक संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए विशेष सुरक्षा दी है, ताकि वैश्विक बाज़ार की मार सीधे किसान पर न पड़े।
खेती के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र को लेकर उठ रहे सवाल और भी अधिक भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों हैं, क्योंकि भारत की दुग्ध उत्पादन व्यवस्था पूरी तरह छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने का तमगा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या औद्योगिक फार्मिंग मॉडल की देन नहीं, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की मेहनत का परिणाम है, जिनके लिए दो-चार पशु आय का स्थायी स्रोत हैं। गांवों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन का जो नेटवर्क विकसित हुआ है, उसने न केवल किसानों को स्थिर आय दी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी मज़बूत किया। यदि अमेरिकी डेयरी उत्पाद, जैसे दूध पाउडर, बटर या अन्य प्रोसेस्ड आइटम, सस्ते दामों पर भारतीय बाज़ार में उतरते हैं, तो यह पूरा संतुलन बिगड़ सकता है और सहकारी मॉडल को गहरी चोट पहुंच सकती है।
आर्थिक विश्लेषणों में यह आशंका बार-बार सामने आई है कि अमेरिकी डेयरी उद्योग की विशाल उत्पादन क्षमता और कम लागत भारतीय छोटे उत्पादकों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है। कुछ आकलनों के अनुसार यदि डेयरी सेक्टर को पूरी तरह खोल दिया गया, तो भारतीय दुग्ध उत्पादकों को हर वर्ष एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूध की कीमतों में संभावित पंद्रह प्रतिशत तक की गिरावट के रूप में ज़मीनी स्तर पर दिखाई देगा। इसका सीधा अर्थ यह होगा कि जिन परिवारों के लिए दूध बिक्री रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने का साधन है, उनकी आय में अचानक कमी आ जाएगी। ऐसे में गांवों की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, जिससे रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी असर पड़ेगा।
इस पूरी बहस को और तीखा बनाने वाला पहलू अमेरिका के कृषि मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के वे बयान हैं, जिनमें भारत की विशाल आबादी को अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़े बाज़ार के रूप में पेश किया गया। इन बयानों को केवल व्यापारिक उत्साह के रूप में देखने के बजाय कई विश्लेषक रणनीतिक दबाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप के दावे और ट्वीट भी चर्चा में आए हैं, हालांकि उनके बयान पहले भी कई बार विवाद और अतिशयोक्ति का विषय रहे हैं। बावजूद इसके, इस बार मामला इसलिए गंभीर माना जा रहा है क्योंकि केवल एक नेता नहीं, बल्कि अमेरिका के कृषि प्रशासन से जुड़े अन्य लोग भी इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। भारत की ओर से इस मुद्दे पर लंबे समय तक चुप्पी रहना, सवालों को और गहरा कर रहा है।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज़ है कि यदि खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी ढील दी गई, तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की उस छवि पर भी पड़ेगा, जिसने खुद को किसान हितैषी और आत्मनिर्भर भारत का पक्षधर बताया है। विपक्ष पहले ही यह सवाल उठा रहा है कि क्या “अमेरिका फर्स्ट” की नीति के सामने “मेक इन इंडिया” और “इंडिया फर्स्ट” को पीछे धकेला जा रहा है। जनता के बीच भी यह चिंता गहराने लगी है कि कहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के नाम पर देश की आंतरिक प्राथमिकताओं से समझौता तो नहीं किया जा रहा। यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि खेती और डेयरी केवल आर्थिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए हैं।

खेती से जुड़े एक और अहम पहलू पर भी बहस तेज़ है, वह है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का सवाल। अमेरिका के कृषि निर्यात में जीएम मकई और जीएम सोयाबीन जैसे उत्पादों की बड़ी हिस्सेदारी है, जबकि भारत में खाद्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा को लेकर इन फसलों पर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। यदि किसी व्यापार समझौते के तहत ऐसे उत्पादों को भारतीय बाज़ार में अनुमति दी जाती है, तो यह केवल आयात का मामला नहीं रहेगा, बल्कि देश की कृषि नीति, बीज स्वायत्तता और पारंपरिक खेती की विविधता पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। किसान संगठनों का कहना है कि एक बार जीएम उत्पादों का रास्ता खुला, तो स्थानीय बीजों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे दीर्घकाल में किसानों की निर्भरता बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बढ़ सकती है।
डेयरी क्षेत्र में आर्थिक नुकसान के साथ-साथ एक सांस्कृतिक विवाद भी उभर कर सामने आया है, जिसे “नॉन-वेज़ दूध” के नाम से जाना जा रहा है। अमेरिका के कई डेयरी फार्म में पशुओं को मांस-आधारित चारा देने की प्रथाएँ अपनाई जाती हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से मेल नहीं खातीं। भारत में दूध को केवल पोषण का स्रोत नहीं, बल्कि शुद्धता और आस्था से जुड़ा उत्पाद माना जाता है। यदि ऐसे उत्पाद भारतीय बाज़ार में प्रवेश करते हैं, तो सामाजिक विरोध और उपभोक्ता असंतोष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह विवाद बताता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते केवल आर्थिक समीकरण नहीं होते, बल्कि उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संभावित असर की बात करें तो खेती और डेयरी में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव शहरों तक महसूस किया जा सकता है। यदि किसानों की आय में गिरावट आती है, तो इसका असर उनकी क्रय शक्ति पर पड़ेगा, जिससे स्थानीय बाज़ार सुस्त होंगे और रोजगार के अवसर घटेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन बढ़ सकता है, जो पहले से ही शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रहा है। इस दृष्टि से देखें तो खेती और डेयरी को लेकर लिया गया कोई भी फैसला केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस मुद्दे को दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित के संदर्भ में देखने की सलाह दे रहे हैं।
सरकार का पक्ष यह है कि किसी भी संभावित डील में संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और सीधे तौर पर अहम कृषि व डेयरी उत्पादों को मुक्त आयात की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। हालांकि किसान संगठनों और विपक्ष का कहना है कि जब तक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी सामने नहीं आती, तब तक आशंकाएँ बनी रहेंगी। उनका तर्क है कि अतीत में भी कई नीतिगत फैसले धीरे-धीरे लागू किए गए, जिनके प्रभाव बाद में सामने आए। इसलिए इस बार केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस नीति विवरण की मांग की जा रही है, ताकि किसानों को यह भरोसा मिल सके कि उनकी आजीविका से कोई समझौता नहीं होगा।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत अपनी उस परंपरागत नीति पर कायम रहेगा, जिसमें खेती और डेयरी को वैश्विक सौदेबाज़ी से अलग रखा गया था, या फिर बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच इस रुख में बदलाव देखने को मिलेगा। यह निर्णय केवल वर्तमान सरकार के कार्यकाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दशकों तक देश की कृषि दिशा तय करेगा। यदि इस क्षेत्र में असंतुलन पैदा होता है, तो उसे सुधारने में वर्षों लग सकते हैं, जबकि उसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा।
खामोशी के बीच उठते सवाल कभी-कभी सबसे तेज़ आवाज़ बन जाते हैं। कई घंटे और दिनों तक आधिकारिक प्रतिक्रिया न आने से अटकलों को और हवा मिली है। किसान, उपभोक्ता और राजनीतिक दल सभी इस बात पर नज़र लगाए हुए हैं कि सरकार स्पष्ट रूप से क्या रुख अपनाती है। क्या वह यह दोहराएगी कि लक्ष्मण रेखा अब भी अटल है, या फिर वैश्विक व्यापार के दबाव में उसे लचीला बनाने का संकेत देगी। इस सवाल का जवाब केवल भारत-अमेरिका संबंधों को ही नहीं, बल्कि देश के भीतर भरोसे और नीति की विश्वसनीयता को भी परिभाषित करेगा।
अंततः यह पूरा मुद्दा भारत के विकास मॉडल की दिशा पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या विकास का अर्थ केवल बड़े बाज़ारों तक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय समझौतों से है, या फिर उसमें उन करोड़ों छोटे किसानों और ग्रामीण परिवारों की सुरक्षा भी शामिल है, जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। खेती और डेयरी के बिना भारत की कल्पना अधूरी है, और यही कारण है कि इस पर लिया गया हर फैसला इतिहास में दर्ज होगा। देश आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से आगे का रास्ता केवल व्यापारिक लाभ से नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय आत्मसम्मान से तय होगा, और यही इस बहस का सबसे गहरा और निर्णायक पहलू है।