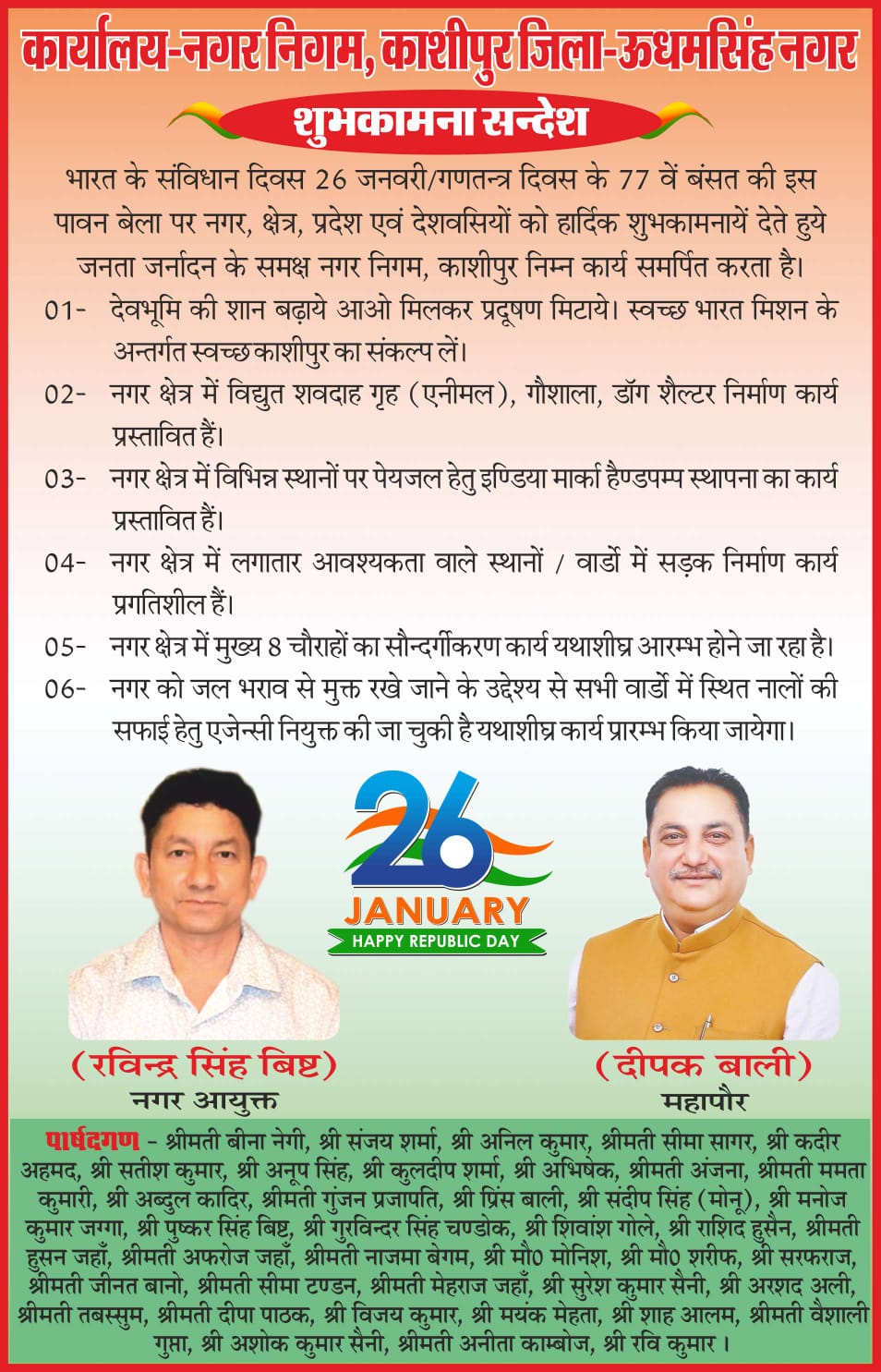रामनगर(सुनील कोठारी)। भारत की राजनीति में धर्म और सत्ता का संबंध हमेशा से एक जटिल, संवेदनशील और बहुस्तरीय विषय रहा है, जहां आस्था, विचारधारा और शासन की सीमाएं अक्सर एक-दूसरे में घुलती हुई दिखाई देती हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश की राजनीतिक यात्रा में शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जब धर्म पूरी तरह राजनीति से अलग रहा हो या राजनीति ने धर्म को पूरी तरह नजरअंदाज किया हो। भारतीय समाज की संरचना, उसकी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक अनुभवों ने इस रिश्ते को लगातार प्रभावित किया है। यही कारण है कि भारत में बार-बार यह सवाल उठता रहा है कि क्या राजनीति धर्म को साधती है या धर्म राजनीति की दिशा तय करता है। इसी बहस के बीच “सॉफ्ट हिंदुत्व” और “हार्ड हिंदुत्व” जैसे शब्द प्रचलन में आए, जिन्होंने राजनीतिक विमर्श को और अधिक धार दी। समय-समय पर अलग-अलग राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे सत्ता प्राप्ति या सत्ता बनाए रखने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, जबकि वे स्वयं इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या बहुसंख्यक समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति बताते हैं।
राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि देश के विभाजन के बाद हिंदू और मुस्लिम पहचानें राजनीति के केंद्र में आ गईं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही किसी न किसी रूप में इस द्वंद्व से प्रभावित रहे। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले जनसंघ और बाद में गठित भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को अपनी राजनीतिक पहचान का प्रमुख आधार बनाया। वर्ष 1980 में जब अटल बिहारी वाजपेई ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, तब उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद जैसे शब्दों का उल्लेख किया था, जिससे यह संकेत मिलता था कि पार्टी एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहती है। हालांकि, कुछ ही वर्षों में यह प्रयोग पीछे छूट गया और देश ने एक ऐसे आंदोलन को देखा जिसने राजनीति की दिशा ही बदल दी। अयोध्या आंदोलन, बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद उभरी कमंडल की राजनीति ने न केवल भाजपा को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर दिया।
इस आंदोलन के बाद भाजपा का राजनीतिक सफर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूपों में सामने आया। कहीं यह तेज आक्रामकता के साथ उभरा तो कहीं इसे सामाजिक स्वीकृति पाने में समय लगा। समय के साथ पार्टी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया कि उसे मुस्लिम वोटों की राजनीति में रुचि नहीं है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में चर्चा हिंदू-मुस्लिम समीकरण से आगे निकलकर खुद हिंदू समाज के भीतर उभरते मतभेदों पर केंद्रित हो गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में वह स्थिति सामने आई है, जहां एक ओर भाजपा की सबसे मजबूत पहचान माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी ओर सनातन परंपरा के सर्वाेच्च धार्मिक पदों में गिने जाने वाले शंकराचार्य। यह टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरे सवाल खड़े कर रहा है।
योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर अपने आप में असाधारण माना जाता है। गोरखपीठ से निकलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ को लंबे समय तक हिंदुत्व की राजनीति का एक मजबूत प्रतीक माना गया। उनकी वेशभूषा, जीवनशैली और सार्वजनिक वक्तव्य उन्हें पारंपरिक राजनेताओं से अलग पहचान देते हैं। संघ और भाजपा के भीतर भी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया, जो हिंदुत्व के मुद्दों को बिना झिझक सामने रख सकता है। वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय किया जा रहा था, तब दिल्ली में मनोज सिन्हा के नाम की चर्चा थी, लेकिन संघ के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने जिस तरह से प्रशासनिक सख्ती, कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक मुद्दों पर फैसले लिए, उससे वे पार्टी और संघ के भीतर लोकप्रिय भी हुए।
हालांकि, समय के साथ हालात बदलते दिखाई देने लगे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटनाओं ने इस पूरी राजनीति को एक नई दिशा दे दी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद अचानक सुर्खियों में आ गया। प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए, उनकी पहचान पर सवाल उठाए गए और यहां तक कहा गया कि उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार किया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने संत समाज और शंकराचार्यों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना था कि शंकराचार्य की पहचान का फैसला कोई प्रशासन या सरकार नहीं कर सकती, यह अधिकार केवल शंकराचार्य परंपरा के पास है। उनका यह बयान सीधे तौर पर सत्ता के अहंकार पर सवाल खड़ा करता है।

यह विवाद यहीं नहीं रुका। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानानंद सरस्वती, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और श्रृंगेरी मठ के स्वामी भारती तीर्थ जैसे प्रमुख धर्माचार्य भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए। कई शंकराचार्यों ने प्रशासन से माफी की मांग की और कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और धार्मिक संस्थाओं का अपमान है। संत समाज ने यहां तक संकेत दिए कि यदि जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह खामोशी अपने आप में इस बात का संकेत है कि मामला साधारण नहीं है और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने धर्म और राजनीति के उस महीन धागे को उजागर कर दिया है, जो अब तक काफी मजबूती से जुड़ा हुआ माना जाता था। एक ओर वह राजनीति है, जिसने हिंदुत्व को सत्ता का माध्यम बनाया, और दूसरी ओर वही हिंदुत्व की धार्मिक परंपराएं हैं, जो अब सत्ता से सवाल कर रही हैं। शंकराचार्य जैसे पद को सनातन परंपरा में भगवान शिव के समान दर्जा दिया जाता है। ऐसे में यदि उनके शिष्यों के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार होता है, तो यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह जाती, बल्कि आस्था और सम्मान का प्रश्न बन जाती है। यही कारण है कि यह विवाद तेजी से राजनीतिक दायरे से निकलकर सामाजिक और धार्मिक विमर्श का केंद्र बन गया है। इस टकराव के बीच एक और पहलू भी उभरकर सामने आया है, जिस पर शंकराचार्यों ने खुलकर बात की है। वह पहलू है गौ रक्षा और उससे जुड़ा आर्थिक पक्ष। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के समय संत समाज को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर सख्ती से रोक लगेगी। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया कि जब देश दुनिया में बीफ के निर्यात में भारत शीर्ष देशों में शामिल हो गया है, तब यह कैसे संभव है कि गौ रक्षा के दावे और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर हो। उन्होंने बीफ निर्यात के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीति में धन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह समझना जरूरी है कि पूंजी कहां से आ रही है और किस कीमत पर।
यह सवाल केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। विपक्षी दल, जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना जैसे दल शामिल हैं, इस मुद्दे को लेकर भाजपा और योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि यह पहली बार है जब हिंदुत्व की राजनीति अपने ही धार्मिक आधार से टकरा रही है। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि धर्म का उपयोग सत्ता के लिए करना और फिर उसी धर्म के प्रतिनिधियों को अपमानित करना एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि चारों शंकराचार्य दिल्ली पहुंचते हैं और संत समाज एकजुट होकर विरोध करता है, तो इसका असर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा।
इतिहास के पन्ने पलटें तो यह पहली बार नहीं है जब सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की बहस तेज हुई हो। इंदिरा गांधी के दौर में भी धर्म और राजनीति के रिश्ते को एक अलग तरीके से साधा गया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को “हिंदू संत” के बजाय “भारतीय संत” के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाई, जिससे एक व्यापक राष्ट्रीय पहचान बनाई जा सके। इसके विपरीत, वर्तमान दौर में हिंदुत्व की राजनीति अधिक स्पष्ट और आक्रामक रूप में सामने आई है। यही कारण है कि जब उसी हिंदुत्व के भीतर से विरोध की आवाज उठती है, तो वह सत्ता के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाती है।
आज की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह टकराव योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करेगा या यह केवल एक अस्थायी विवाद बनकर रह जाएगा। संत समाज की भूमिका, शंकराचार्यों की एकजुटता और संघ परिवार की प्रतिक्रिया आने वाले समय में इस सवाल का जवाब दे सकती है। इतना तय है कि धर्म और राजनीति की यह जटिल लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा। यदि संवाद और सम्मान का रास्ता नहीं चुना गया, तो यह टकराव उस राजनीति की नींव को भी हिला सकता है, जिसने पिछले दशकों में हिंदुत्व के सहारे अपनी सबसे मजबूत पहचान बनाई है।