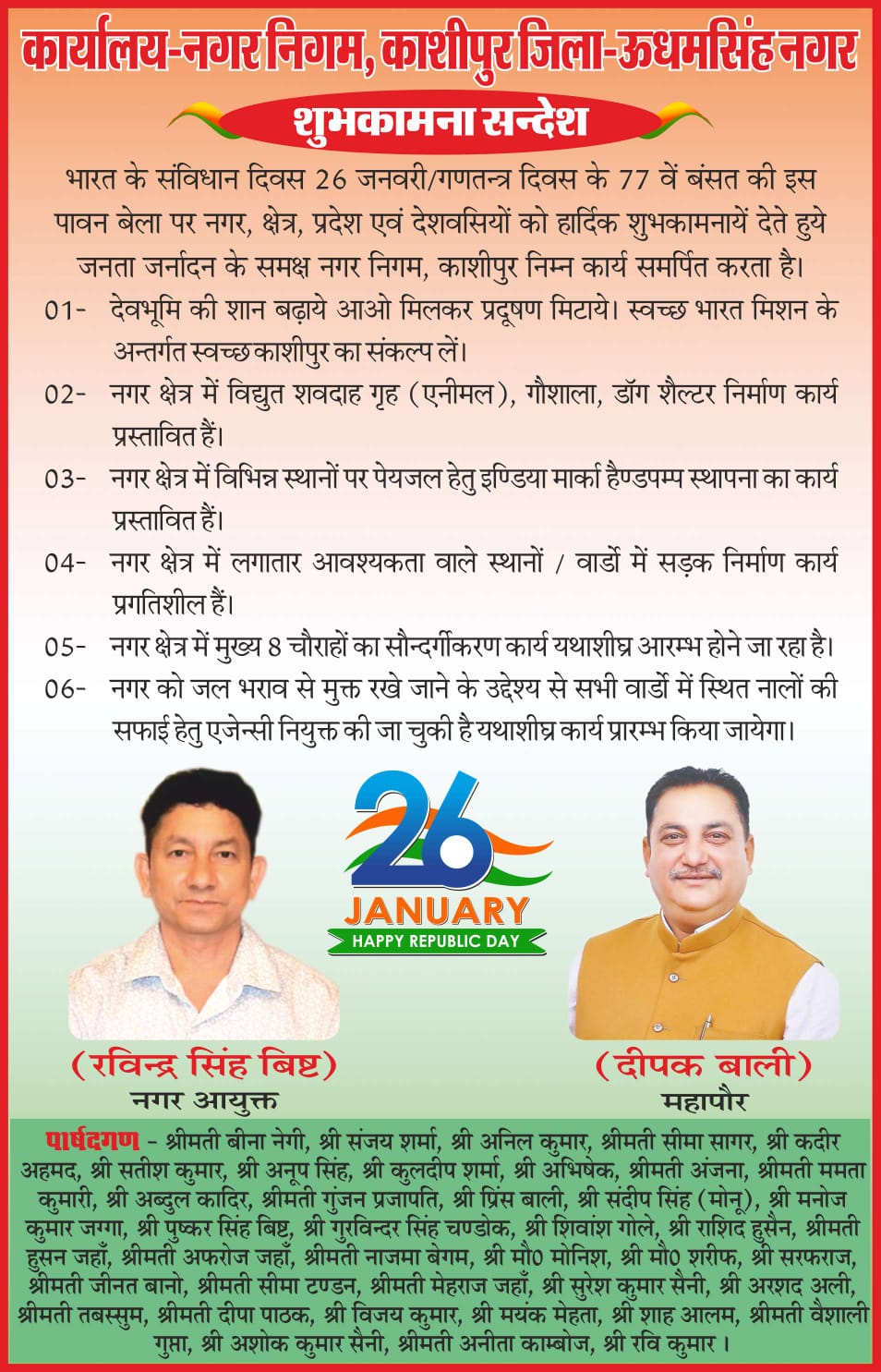नई दिल्ली(सुनील कोठारी)। अमेरिका को ईस्ट इंडिया कंपनी की छाया में देखना आज की दुनिया की सटीक तस्वीर नहीं है, और भारत भी अब रियासतों का बिखरा हुआ समूह नहीं बल्कि एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक ढांचा है, जहां चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रधानमंत्री और संवैधानिक संस्थाएं हैं। उसी तरह अमेरिका के भीतर भी राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है और वहां की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक परंपराओं से संचालित होती है। एक ओर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरी ओर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशकृइन दोनों के संबंध स्वाभाविक रूप से समानता और साझेदारी पर टिके होने चाहिए थे। मगर बदलते वैश्विक परिदृश्य में राजनीति और बाजार का गठजोड़ इस कदर हावी हो चुका है कि हर राष्ट्र अपनी ताकत का प्रदर्शन व्यापार, निवेश और आर्थिक समझौतों के जरिये करने लगा है। इसी पृष्ठभूमि में यह सवाल उभरता है कि भारत ने अमेरिका के साथ ऐसी डील क्यों स्वीकार की, जिसमें संतुलन के बजाय एकतरफा दबाव की बू दिखाई देती है। यह समझौता केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक निहितार्थों से भरा हुआ प्रतीत होता है। पूरे घटनाक्रम ने भारत की स्वायत्तता, नीति-निर्धारण और दीर्घकालिक हितों को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।
वर्तमान समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी कमान पूरी तरह अमेरिका के हाथों में दिखाई देती है। वाइट हाउस से जारी कार्यकारी आदेश न केवल दिशा-निर्देश देता है बल्कि पालन न होने की स्थिति में दंड का प्रावधान भी करता है। शुरुआत में दो पन्नों का संयुक्त बयान सामने आता है, लेकिन उसके बाद जो आदेश जारी हुआ, उसने तस्वीर को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। इस आदेश में यह अधिकार सुरक्षित रखा गया है कि अमेरिका जब चाहे, जिस आधार पर चाहे, इस डील को समाप्त कर सकता है। खासकर तेल और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिका की पैनी निगाह स्पष्ट रूप से दर्ज है। भारत किससे तेल खरीदे, क्यों खरीदे या किससे न खरीदेकृयह तक तय करने का अधिकार इस आदेश के जरिए अमेरिका अपने पास रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार-बार दोहराए गए स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल जैसे नारे अचानक कमजोर पड़ते नजर आते हैं, मानो आत्मनिर्भरता की पूरी अवधारणा एक झटके में किनारे कर दी गई हो।
इस स्थिति ने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला यह कि क्या भारत और अमेरिका की जरूरतें इतनी अलग हैं कि दोनों का नजरिया इस डील को लेकर टकरा रहा है। दूसरा और कहीं अधिक गंभीर सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीतिक सत्ता और आर्थिक स्थिरता अमेरिकी दबावों पर निर्भर होती जा रही है। सत्ता का अर्थ यहां केवल सरकार नहीं बल्कि वह अर्थव्यवस्था भी है, जो बड़े कॉरपोरेट घरानों के सहारे चलती है। वही बड़े उद्योगपति और कारोबारी समूह अब यह महसूस करने लगे हैं कि चीन और रूस की ओर खुलकर झुकना उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। पश्चिमी देशों और खासतौर से अमेरिका के साथ खड़े रहना उन्हें अधिक सुरक्षित विकल्प लगता है। चीन जहां युवान को आगे बढ़ा रहा है और रूस रूबल की बात कर रहा है, वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मोर्चे पर भी सुस्ती दिखाई दे रही है। ऐसे में पूंजी के रास्ते सिमटते नजर आते हैं।
देश के भीतर यह सच्चाई भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत कुछ गिने-चुने हाथों में सिमटती जा रही है। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग पचास बड़े बिजनेस हाउस देश की कुल संपत्ति के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि बहुसंख्यक आबादी सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रही है। जब इतना बड़ा आर्थिक असंतुलन हो, तो नीति-निर्धारण पर भी उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। खनन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे से आगे बढ़कर अब कृषि क्षेत्र तक में कॉरपोरेट दखल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह आशंका गहराती है कि कहीं भारत ने इसी दबाव में अमेरिका के साथ यह समझौता तो नहीं कर लिया। दूसरी ओर अमेरिका की जल्दबाजी भी सवालों के घेरे में है। महज बारह घंटे के भीतर आदेश जारी होना इस बात का संकेत देता है कि वाशिंगटन भारत को किसी भी कीमत पर अपने पाले में बनाए रखना चाहता था।
अमेरिका की चिंता केवल भारत के साथ व्यापार तक सीमित नहीं है। एशिया में उसकी रणनीति कई मोर्चों पर चुनौतियों से घिरी हुई है। भारत यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, ब्रिक्स और आसियान देशों के साथ समानांतर संबंध मजबूत कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के भीतर यह डर था कि यदि भारत हाथ से फिसल गया तो एशिया में उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इजराइल के भरोसे पूरे एशियाई परिदृश्य को साधना संभव नहीं है। इसके अलावा डॉलर की वैश्विक स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। चीन खुले तौर पर युवान को अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का माध्यम बनाने की बात कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत का झुकाव किसी नए आर्थिक ब्लॉक की ओर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी था। यही वजह है कि बदलते विश्व व्यवस्था के इस दौर में अमेरिका ने भारत को केंद्र में रखकर अपनी चाल चली।
सबसे गंभीर पहलू उस कार्यकारी आदेश में दर्ज शर्तें हैं, जिनके तहत भारत ने रूसी फेडरेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके बदले अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने का वादा किया गया है। साथ ही अगले दस वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ाने की सहमति भी शामिल है। इसका अर्थ यह है कि भारत, जो दशकों से रूस से हथियार और सस्ता कच्चा तेल लेता रहा है, अब धीरे-धीरे उस दिशा से हटने को बाध्य होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त विभाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। यदि कहीं यह पाया गया कि भारत ने फिर से रूसी तेल का आयात शुरू किया है, तो अतिरिक्त कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी, जिसमें टैरिफ बढ़ाने जैसे कठोर कदम भी शामिल हो सकते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार के भीतर तालमेल की कमी भी उजागर हुई है। जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से रूस से तेल आयात को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे विदेश मंत्रालय का विषय बताकर किनारा कर लिया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में पूछे गए सवाल पर कहा कि वे इस डील में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं और यह मामला वाणिज्य मंत्रालय देख रहा है। इस तरह दो वरिष्ठ मंत्रियों के बयानों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। दूसरी ओर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोबाल का नाम सामने आया, जिसे बाद में हटा लिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस डील के पीछे रणनीतिक सोच उन्हीं की थी। इस तरह की खबरों का आना और फिर हट जाना भी इस समझौते की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
रूस के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी बड़ा प्रश्न है। क्या मास्को अब नई दिल्ली पर पहले जैसा भरोसा कर पाएगा। चीन भी इस स्थिति को बारीकी से देख रहा है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अगुवाई कर रहा है, जहां वैकल्पिक मुद्रा और डिजिटल करेंसी जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। यदि भारत इन विषयों पर पीछे हटता है, तो यह केवल ब्रिक्स ही नहीं बल्कि एससीओ और आसियान जैसे मंचों पर भी उसकी भूमिका को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच ईरान को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। ओमान में हुई बातचीत विफल रही और यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। ऐसे समय में भारत का अमेरिका के साथ यह समझौता क्षेत्रीय समीकरणों को और जटिल बना देता है।
आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस डील के फायदे और नुकसान दोनों पर गंभीर मंथन जरूरी है। रूस से सस्ता तेल न खरीदने पर 25 प्रतिशत टैरिफ हटना एक राहत की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही लगभग 30 प्रतिशत सस्ते कच्चे तेल का लाभ भी खत्म हो जाता है। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका से खरीदारी रूस की तुलना में कहीं अधिक महंगी है। वेनेजुएला से तेल आयात की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा टैरिफ की दरों में पहले की तुलना में भारी बढ़ोतरी हुई है। जहां कभी 2 से 3 प्रतिशत टैरिफ था, वह बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे निर्यातक उद्योगों की लाभप्रदता पर सीधा असर पड़ेगा और रोजगार सृजन की क्षमता भी घटेगी।
अमेरिका को भारत द्वारा किए गए निर्यात का आंकड़ा भी इस बहस में अहम है। पिछले वर्ष लगभग 86.5 अरब डॉलर का सामान अमेरिका भेजा गया, जिसमें आधे से अधिक निर्यात चार प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित रहा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हीरा-जवाहरात, फार्मा उत्पाद और वस्त्र उद्योग इनमें शामिल हैं। इन क्षेत्रों को कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातकों के लिए परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 30 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बाजार के खुलने की बात कही जा रही है, लेकिन यह बाजार केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए खुला है। यूरोपीय यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भी उसी प्रतिस्पर्धा में हैं।
कृषि क्षेत्र को लेकर भी चिंता कम नहीं है। कार्यकारी आदेश में कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की प्रतिबद्धता का उल्लेख है। गैर-टैरिफ बाधाओं का अर्थ है गुणवत्ता मानकों और परीक्षण प्रक्रियाओं में ढील। इससे अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पाद बिना कड़े परीक्षण के भारतीय बाजार में आ सकते हैं। पशु आहार, खाद्य तेल और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को लेकर पहले से मौजूद आपत्तियां कमजोर पड़ सकती हैं। इसका सीधा असर भारतीय किसानों और स्थानीय उत्पादकों पर पड़ेगा, जो पहले ही उत्पादन लागत और बाजार असमानता से जूझ रहे हैं। यह स्थिति धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र में भी कॉरपोरेट प्रभुत्व को मजबूत कर सकती है।
इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखने पर यह सवाल और गहराता है कि क्या भारत की संप्रभुता और नीति-स्वतंत्रता इस समझौते में दांव पर लगी है। जिस तरह अमेरिका ने निगरानी और दंड की व्यवस्था बनाई है, उससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में भी दबाव की राजनीति जारी रह सकती है। आज एक अनुकूल मानचित्र जारी होने पर खुशी मनाई जा रही है, लेकिन यदि कल परिस्थितियां बदलीं तो वही समर्थन सवालों में बदल सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल हित होते हैं। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी है कि वह संतुलन बनाए रखे और किसी एक ध्रुव पर पूरी तरह निर्भर न हो।
अंततः यह पूरा मामला केवल एक व्यापारिक समझौते का नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक दिशा का है। क्या देश अपनी आर्थिक नीतियों को बाहरी दबावों के अनुरूप ढालता रहेगा या फिर आत्मनिर्भरता और संतुलित कूटनीति के रास्ते पर लौटेगा। संसद के भीतर और बाहर इस पर खुली बहस जरूरी है। मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जहां आलोचनात्मक दृष्टि के बजाय सरकारी बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। पांच बड़े सवालकृडॉलर की निर्भरता, कॉरपोरेट प्रभाव, रोजगार का भविष्य, अंतरराष्ट्रीय संतुलन और संप्रभुताकृअब भी जवाब मांगते हैं। इन सवालों के उत्तर ही तय करेंगे कि यह डील भारत के लिए अवसर है या आने वाले समय का संकट।