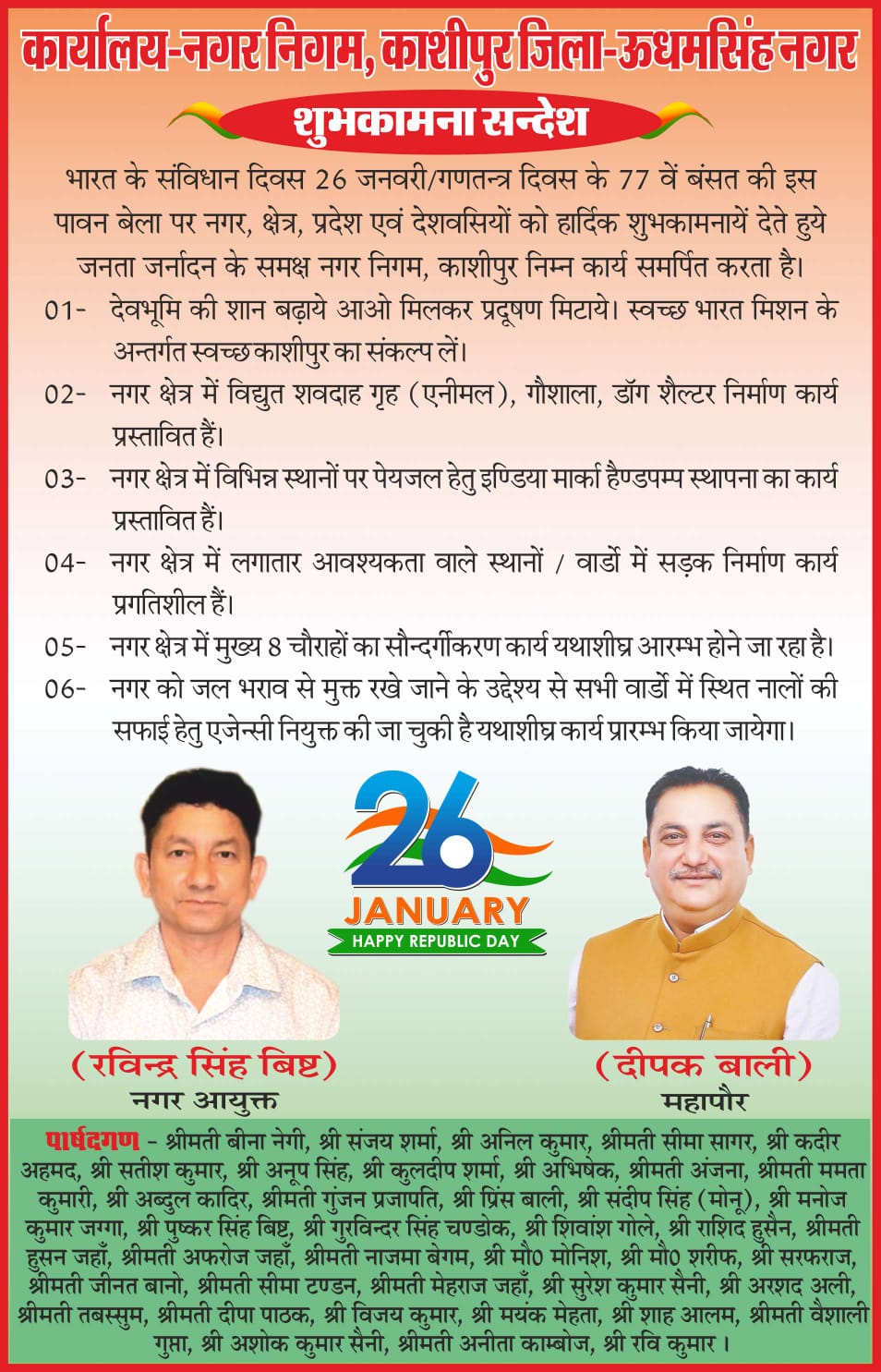नई दिल्ली(सुनील कोठारी)। समकालीन भारतीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के परिदृश्य में जो उथल-पुथल इन दिनों दिखाई दे रही है, उसने देश की दिशा और दशा दोनों को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बीते कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंध जिस तेज़ी से सुर्खियों में आए हैं, वह केवल द्विपक्षीय मित्रता या रणनीतिक साझेदारी का मामला भर नहीं रह गया है, बल्कि उसमें आर्थिक दबाव, व्यापारिक शर्तें, ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक छवि जैसे कई गहरे आयाम जुड़ गए हैं। इन्हीं आयामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वह किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय दबाव में आ गए हैं, जिसने भारत की परंपरागत स्वतंत्र विदेश नीति को कमजोर कर दिया है। यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इन चर्चाओं की शुरुआत किसी आधिकारिक भारतीय बयान से नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक दावों से हुई, जिन्होंने एकतरफा अंदाज़ में यह बताने की कोशिश की कि भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
राजनीतिक गलियारों में इस बहस को और धार तब मिली, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर “कॉम्प्रोमाइज्ड” होने का आरोप लगाया। उनका यह बयान केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं माना गया, बल्कि इसे भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़ा करने वाली टिप्पणी के रूप में देखा गया। राहुल गांधी का कहना था कि बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उनमें भारत सरकार की चुप्पी और अमेरिका की मुखरता यह संकेत देती है कि फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं और देश को बाद में उनकी जानकारी दी जा रही है। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी चिंताजनक मानी जा रही है, क्योंकि संसद के भीतर इन मुद्दों पर खुली चर्चा का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट ने इस पूरे विवाद को वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। उन्होंने यह लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक समझौतों पर चर्चा हुई। इसी पोस्ट में यह दावा भी किया गया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से अधिक ऊर्जा संसाधन खरीदेगा। इस बयान ने भारत की दशकों पुरानी रूस नीति पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक रूस भारत का एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है। रक्षा से लेकर ऊर्जा तक, दोनों देशों के संबंध केवल व्यापारिक नहीं बल्कि भू-राजनीतिक संतुलन से जुड़े रहे हैं।
इन दावों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि भारत सरकार की ओर से तत्काल और स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। आमतौर पर संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मामलों में विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इससे यह धारणा बनी कि शायद अमेरिका के बयान को नकारने या संशोधित करने की स्थिति में भारत नहीं है। इसी चुप्पी ने विपक्ष को यह कहने का अवसर दिया कि देश की नीतियां किसी बाहरी दबाव में तय की जा रही हैं और जनता को वास्तविक तस्वीर से दूर रखा जा रहा है।
व्यापारिक संबंधों का मुद्दा इस बहस का केंद्र बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को लगभग पूरी तरह खोलने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह बदलाव इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि अब तक भारत के निर्यात पर औसतन 2 से 4 प्रतिशत का ही टैरिफ लगता रहा है। अचानक इतनी बड़ी वृद्धि से भारत के निर्यातकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेष रूप से टेक्सटाइल और हीरा उद्योग, जो पहले ही वैश्विक मंदी और घरेलू संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह फैसला मुश्किलें और बढ़ा सकता है।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी चर्चा के केंद्र में आ गई। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए यह कहा कि “मेड इन इंडिया” उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगने की घोषणा से भारत खुश है। इस बयान को लेकर सवाल उठे कि क्या सरकार इस बढ़े हुए टैरिफ को वास्तव में उपलब्धि मान रही है या यह केवल कूटनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा है। आलोचकों का तर्क है कि जब किसी देश के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया जाए, तो उसे सकारात्मक उपलब्धि के रूप में पेश करना समझ से परे है। इससे यह संदेह और गहराया कि कहीं सरकार किसी बड़े दबाव को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही।
इस पूरे घटनाक्रम में कृषि क्षेत्र को लेकर उठी आशंकाएं भी कम गंभीर नहीं हैं। अमेरिकी कृषि मंत्री द्वारा यह कहना कि अमेरिकी किसानों के उत्पाद अब भारतीय बाजार में पहुंचेंगे, सीधे तौर पर भारत के करोड़ों किसानों की आजीविका से जुड़ा सवाल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कई मौकों पर यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने कृषि बाजार को विदेशी दबाव में नहीं खोलेगा और किसानों के हित सर्वोपरि रहेंगे। ऐसे में अमेरिका की ओर से किए गए दावे और भारत की ओर से उस पर कोई आपत्ति न जताया जाना, इन बयानों के साथ टकराव पैदा करता है।
राजनीतिक दृष्टि से यह मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि संसद में इस पर चर्चा की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, जबकि वह चीन, सीमा सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों के विरोधाभास को सामने रखना चाहते थे। उनका यह कहना कि प्रधानमंत्री की छवि पर सवाल उठने के डर से सरकार बहस से बच रही है, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को और तीखा बना रहा है। इस दौरान गृह मंत्री की अनुपस्थिति और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे, जिससे यह धारणा बनी कि सत्ता पक्ष किसी भी तरह इस मुद्दे को संसद के भीतर आने से रोकना चाहता है।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह पूरा विवाद केवल भारत-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद, रूस के साथ ऐतिहासिक मित्रता और पश्चिम एशिया में बदलते समीकरण, इन सबके बीच भारत की संतुलनकारी भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। ऐसे समय में यदि यह संदेश जाता है कि भारत किसी एक शक्ति के दबाव में अपनी नीतियां बदल रहा है, तो इसका असर उसकी वैश्विक साख पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस बहस को केवल घरेलू राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है।
इस तरह, मौजूदा परिस्थितियां कई सवाल छोड़ती हैं। क्या भारत वास्तव में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए यह समझौते कर रहा है, या फिर परिस्थितियों ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे “कॉम्प्रोमाइज्ड” होने के आरोप महज राजनीतिक हैं, या उनके पीछे कोई ठोस वजह है? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में यह मुद्दा भारतीय राजनीति और कूटनीति दोनों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।